स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी
- बाला लखेंद्र
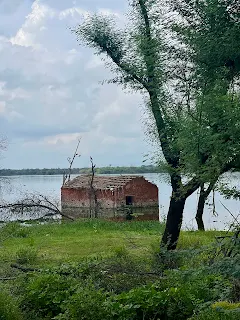 शोध सार : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन कई भागों में बंटा हुआ एक पूर्ण मानव की सम्पूर्णता की तलाश का एक विलक्षण उदाहरण है। अपने बाल्य-काल से ही सत्य के प्रति आत्मिक चेतना को जागृत करते हुए गांधी एक असाधारण और कठिन राह का अनुसरण करने वाले एक महान साधक के रूप में हमें मिलते हैं। वकालत की दुनिया से निकलकर भारत की स्वतंत्रता का अलख जगाने वाला महानायक मोहन दस करमचन्द गांधी अपने जीवन को कई महत्वपूर्ण आयामों से उभरते हुए दीख पड़ते हैं। वे जीवन भर एक सत्याग्रही के रूप में सत्य के प्रयोग में सिद्धांत रूप से शामिल होते हैं, जिसे हम उनकी पुस्तक "माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ" में महसूस कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन और उनकी पत्रकारिता का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विषय पर चर्चा हुई तो है पर उसे विस्तार नहीं मिल पाया है। गांधी जी द्वारा अपने जीवन के नैतिक मूल्यों ‘सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, उपवास, सर्वोदय आदि विषयों पर तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों, संपादकीय तथा लेखों की अभिव्यक्ति के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन हुए हैं परन्तु गांधी जी एक पत्रकार के रूप में स्वयं चिंतन की कौन सी धारा अपनाते हैं, इसका अध्ययन आवश्यक है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में महात्मा गांधी के कार्य-कलापों के साथ-साथ अपने धुन की छवि का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता संग्राम के इस महायज्ञ में समर्पित व समर्थित अनेक पत्र-पत्रिकाओं के समर्थन के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता का अमूल्य योगदान का अध्ययन करना इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य है। भारतीय स्वाधीनता की संघर्ष चेतना को जागृत करते हुए व्यापक स्तर पर अपने सशक्त विचारों को जन- जन तक पहुंचाने का काम गांधी जी बड़े ही सहज और सरल तरीके से करने हेतु प्रयासरत रहे और सफल भी हुए। गांधी जी का यह कार्य, राष्ट्रहित के लिए समर्पित, निडर एवं निर्भीक पत्रकारों को एक नई दिशा प्रदान करने में सफल रहा जिसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिफल, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता है।
शोध सार : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन कई भागों में बंटा हुआ एक पूर्ण मानव की सम्पूर्णता की तलाश का एक विलक्षण उदाहरण है। अपने बाल्य-काल से ही सत्य के प्रति आत्मिक चेतना को जागृत करते हुए गांधी एक असाधारण और कठिन राह का अनुसरण करने वाले एक महान साधक के रूप में हमें मिलते हैं। वकालत की दुनिया से निकलकर भारत की स्वतंत्रता का अलख जगाने वाला महानायक मोहन दस करमचन्द गांधी अपने जीवन को कई महत्वपूर्ण आयामों से उभरते हुए दीख पड़ते हैं। वे जीवन भर एक सत्याग्रही के रूप में सत्य के प्रयोग में सिद्धांत रूप से शामिल होते हैं, जिसे हम उनकी पुस्तक "माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ" में महसूस कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन और उनकी पत्रकारिता का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विषय पर चर्चा हुई तो है पर उसे विस्तार नहीं मिल पाया है। गांधी जी द्वारा अपने जीवन के नैतिक मूल्यों ‘सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, उपवास, सर्वोदय आदि विषयों पर तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों, संपादकीय तथा लेखों की अभिव्यक्ति के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन हुए हैं परन्तु गांधी जी एक पत्रकार के रूप में स्वयं चिंतन की कौन सी धारा अपनाते हैं, इसका अध्ययन आवश्यक है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में महात्मा गांधी के कार्य-कलापों के साथ-साथ अपने धुन की छवि का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता संग्राम के इस महायज्ञ में समर्पित व समर्थित अनेक पत्र-पत्रिकाओं के समर्थन के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता का अमूल्य योगदान का अध्ययन करना इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य है। भारतीय स्वाधीनता की संघर्ष चेतना को जागृत करते हुए व्यापक स्तर पर अपने सशक्त विचारों को जन- जन तक पहुंचाने का काम गांधी जी बड़े ही सहज और सरल तरीके से करने हेतु प्रयासरत रहे और सफल भी हुए। गांधी जी का यह कार्य, राष्ट्रहित के लिए समर्पित, निडर एवं निर्भीक पत्रकारों को एक नई दिशा प्रदान करने में सफल रहा जिसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिफल, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता है।बीज शब्द : पत्रकारिता, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण, सत्याग्रह, सर्वोदय, राष्ट्रीय चेतना,भारत राष्ट्र, भारतीय राजनीति, प्रतिनिधि, सांस्कृतिक जागरण।
मूल आलेख : बहुत कम लोग जानते हैं कि हिन्दी पत्रकारिता में जो काल-विभाजन किया गया है, उसमें सन् 1920 से 1947 तक का युग 'गांधी युग' कहा जाता है। इन 27 वर्षों में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम और असहयोग आंदोलन के प्रसार के लिए देश में अनेक दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्रों का प्रकाशन हिन्दी में प्रारम्भ हुआ। इस युग की पत्रकारिता पर गांधी जी का विशेष प्रभाव रहा। श्री रामनारायण चौधरी ने गांधी युग के संदर्भ में लिखा है कि "गांधी युग के दौरान अधिकांश समाचार पत्र राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर निकलने लगे थे तथा गांधी जी की नैतिक प्ररेणा और उनके स्वयं के प्रभाव से उक्त पत्रकारों ने अपने लिए आचार संहिता भी स्वयं निर्धारित कर ली थी।"[1]
जब गांधी लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों वे "डेली न्यूज", "डेली टेलीग्राफ" और "पालमाल गजट" आदि समाचार पत्रों से काफी प्रभावित हुए। वे इन समाचार पत्रों का नियमित तौर पर अध्ययन किया करते थे। गांधी जी 1888 में द लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने और सोसाइटी के समाचार पत्र "द वेजीटेरियन" के लिए लिखना आरम्भ किया। उसमें उनके लगभग एक दर्जन लेखों का प्रकाशन हुआ। एक तरह से कानून की शिक्षा के साथ गांधीजी की पत्रकारिता का यह प्रशिक्षण काल था, जो 1888 से शुरू होकर 1891 तक चला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक व्यवस्था की रिपोर्टिंग के लिए "द वेजिटेरियन" का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। "द वेजिटेरियन" में उनका पहला लेख "भारतीय अन्नाहारी (इंडियन वेजीटेरियन), 7 फरवरी 1891 तथा भारतीय त्योहार (सम इंडियन फेस्टिवल्स), 28 फरवरी 1891 में प्रकाशित हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब महात्मा गांधी स्वदेश लौटे तो उन्होंने अपनी पहली यात्रा-कथा (ऑन माय वे होम अगेन टू इंडिया) शीर्षक से दो लेख "द वेजीटेरियन" को भेजा जो क्रमशः 9 और 16 अप्रैल 1892 को "द वेजीटेरियन" में प्रकाशित हुआ। [2]
अफ्रीका में 3 वर्षों तक रहकर महात्मा गांधी ने वकील से ज्यादा पत्रकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। अप्रैल 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए और वहाँ की रंगभेद की अमानवीयता ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। दादा भाई अब्दुल्ला के प्रिटोरिया वाले मुकदमे के बाद महात्मा गांधी डरबन गए, जहां "नेटाल मरकरी' अखबार से परिचित होकर उन्होंने भारतीयों को मताधिकार से वंचित कराए जाने पर चिंता प्रकट की। उनकी सक्रियता के कारण 1894 में मताधिकार विधेयक विरोध प्रस्ताव से संदर्भित आठ लेख लंदन के "टाइम्स" द्वारा प्रकाशित किया गया। "भारतीय मताधिकार" शीर्षक अखबारी पैराग्राफ गांधी जी की सक्रियता का एक प्रमुख अभिलेख माना जाता है। गांधीजी मानव सेवा के लिए पत्रकारिता को एक अचूक और प्रमुख शस्त्र के रूप में देखते थे। [3] अफ्रीका से प्रकाशित "प्रिटोरिया न्यूज", "नेटाल मरकरी नंदाल एडवरटाइजर" से जुड़कर उन्होंने भारतीयों और मानव हित से संबंधित कई लेख लिखे जिसे इंग्लैंड से प्रकाशित किया गया। "इंडिया", डरबन, जोहान्सबर्ग के संवाददाता के रूप में गांधीजी ने अफ्रीका में चल रहे मानव संघर्ष को अपनी लेखनी से उजागर किया। "इंडिया" दादा भाई नौरोजी द्वारा 1890 में निकाला गया था। 14 अगस्त 1896 को स्वदेश लौटने पर राजकोट में रहकर महात्मा गांधी ने एक महीने "ग्रीवांस ऑफ ब्रिटिश इंडियनस इन साउथ अफ्रीका" नाम की पुस्तिका प्रकाशित की। इलाहाबाद के "पायोनियर" ने सर्वप्रथम इस पोथी पर टिप्पणी लिखी, जिसे दूसरे अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा।
"ग्रीन पैम्फलेट" के कारण "मद्रास स्टैंडर्ड" के संपादक जी. पी. पिल्ले, "हिंदू" के संपादक, जी. सुब्रमण्यम, "इग्लिशमैन" के संपादक, मि. सांडर्स महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित हुए। "द वेजीटेरियन" (1891) और ग्रीन पैम्फलेट (1896) ने गांधी की रचनात्मक और संघर्षात्मक पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की। गांधी ने 1899 ईस्वी में बोअर युद्ध के समय एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में युद्ध के मैदान से "टाइम्स ऑफ इंडिया" के लिए रिपोर्टिंग की। "प्रिटोरिया न्यूज" के संपादक नि. वियर स्टेंट ने महात्मा गांधी द्वारा युद्ध स्थल से भेजे गए चित्र और रिपोर्टिंग को प्रकाशित की। गांधी ने वर्णनात्मक पत्रकारिता की नीरसता को तोड़ा और शायद यही कारण है कि "मॉर्निंग पोस्ट" में कार्यरत युद्ध संवाददाता मि. चर्चिल उनकी अभिव्यक्ति और प्रतिभा के कायल हो गए। "केपटाइम्स" अखबार ने गांधीजी के बारे में लिखा "यह भारतीय जहां भी जाता है, काफी अच्छा और उपयोगी काम करता है।“[4]
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने विशिष्ट समाजसेवी और पत्रकारों से संपर्क किया। जीवन यात्रा के प्रारंभिक दिनों की अपनी अनुभूति को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया, "यहाँ से मैं गोखले के पास गया। वे फर्मयुसन कॉलेज में थे। गोखले ने बारीकी से मेरी जांच की। मुझसे बड़े प्रेम से मिले और मुझे अपना बना लिया। उन्होंने बताया कि मैं किस-किस से और कैसे मिलूं और मेरा भाषण देखने को मांगा। मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई। जब जरूरत हो तब मुझे मिलने को कहा और विदा किया। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले ने जीते जी मेरे हृदय में प्राप्त किया और स्वर्गवास बाद आज भी जो स्थान उन्हें प्राप्त है, वह और कोई पा नहीं सका। यहां मद्रास में मुझे बड़ी से बड़ी मदद स्वर्गीय जी. परमेश्वरन पिल्ले से मिली। वह "मद्रास स्टैंडर्ड" के संपादक थे। "हिंदू" के जी सुब्रमण्यम से भी मैं मिला। उन्होंने मुझे अपने समाचार पत्र का मनचाहा उपयोग करने का अवसर दिया और मैंने निसंकोच उसका उपयोग भी किया। "स्टेट्समैन" और "इंग्लिशमैन" दोनों दक्षिण अफ्रीका के सवाल का महत्व समझते थे। उन्होंने लंबी मुलाकाते छापी। इंग्लिशमैन के मिस्टर सांडर्स ने मुझे अपनाया। मुझे उनके दफ्तर और अखबार का उपयोग करने की पूरी अनुकूलता प्राप्त हो गई। उन्होंने अपने अग्रलेख में काट-छांट करने की भी मुझे छूट दे दी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे बीच स्नेह का संबंध स्थापित हो गया। उन्होंने मुझे वचन दिया जो मदद उनसे हो सकेगी वे करते रहेंगे। मेरे दक्षिण अफ्रीका लौट जाने पर भी उन्होंने मुझसे पत्र लिखते रहने को कहा और वचन दिया कि स्वयं उनसे जो कुछ हो सकेगा, वे करेंगे। मैंने देखा कि इस वचन का उन्होंने अक्षरशः पालन किया, और जब तक ये बहुत बीमार नहीं हो गये मुझसे पत्र व्यवहार करते रहे। मि. सांडर्स को मेरी जो बात अच्छी लगी यह थी आतिश्योक्ति का अभाव और सत्य परायणता। उन्होंने मुझसे जिरह करने में कोई कसर नहीं रखी थी। उसमें उन्होंने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रीका के गोरों के पक्ष को निष्पक्ष भाव से रखने में और भारतीय पक्ष से उसकी तुलना करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी थी।" [5]
उन्हीं दिनों "दी क्रिटिक" के उप संपादक मिस्टर पोलक ने महात्मा गांधी को रस्किन की पुस्तक "अन टू द लॉस्ट” भेंट की। इस पुस्तक ने गांधी के संचार प्रभाव को तेज कर दिया और वे पत्र- प्रकाशन की ओर शिद्दत से जुट गए। नेटाल - इंडियन कांग्रेस को मुखरित करने के माध्यम के रूप में "इंडियन ओपिनियन" की अवधारणा उनके मन में आई। श्री मदनजीत ने डरबन में "द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस" की स्थापना की। मनसुखलाल नाचे इसके संपादक बनाए गए हालांकि संपादकीय और अन्य महत्वपूर्ण कार्य गांधी जी के जिम्मे था। इस तरह 24 दिसंबर 1904 को "इंडियन ओपिनियन" का प्रथम अंक अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में छपा। "इंडियन ओपिनियन" के प्रथम अंक में महात्मा गांधी ने लिखा- "भारतीय लोगों पर हुए अत्याचार को प्रदर्शित करना तथा विचारों का प्रसार करना इसका पहला उद्देश्य है जिससे लोगों में सत्यनिष्ठा जागृत हो सके।" [6]
गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, "इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। राजनीतिक संघर्ष में "इंडियन ओपिनियन" की आंदोलनकारी भूमिका थी। रंगभेद की समस्या, भारतीय कला संस्कृति, समानता जैसी बातों पर इसका ध्यान था। [7]
चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर समाचार पत्रों की ताकत को समझते हुए "प्रताप" जिसके सम्पादक, पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी रहे। उसके चंपारण संवाददाता पीर मुहम्मद मुनीस को हमेशा अपने साथ रखा। यह एक संयोग ही था कि महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल ने जिस व्यक्ति से उन्हें पत्र लिखवाया वह पीर मुहम्मद मुनीस ही थे। [8] चम्पारण से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अंग्रेजी साप्ताहिक "यंग इंडिया' का प्रकाशन 7 अक्टूबर 1919 को प्रारंभ किया। 1920 में "यंग इंडिया" असहयोग आंदोलन का प्रमुख समाचार पत्र बन गया। 18 दिसंबर 1920 के अंक में महात्मा गांधी ने घोषित किया की "यंग इंडिया" के कॉलम असहयोग आंदोलन के विरुद्ध मत व्यक्त करने वालों के लिए सदैव खुले हैं। इसके प्रथम पृष्ठ पर बाएं कोने में विषय सूची तथा उसके नीचे नोट्स एंड यूज स्तंभ हुआ करता था। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो तीन टिप्पणियाँ निकलीं, उनके शीर्षक इस प्रकार थे- "नो सिक्योरिटी", "वी आर ऐट टू मिस्टेक्स" और "सिक्स सप्रेस्ड क्लास स्कूल्स इन अहमदाबाद" अंतिम टिप्पणी में प्रोफेसर ध्रुव के अस्पृश्यता संबंधी विचारों की गांधीजी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। [9]
7 सितंबर 1918 को महात्मा गांधी ने गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का संपादन और प्रकाशन अपने हाथ में लिया, जिसका प्रकाशन पहले अहमदाबाद में होता था। 8 अगस्त 1920 के अंक में इस पत्र ने तिलक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जिन्होंने अपनी देह को देश सेवा में ही जीर्ण कर दिया। उनका यह देह समाप्त होने पर भी वे जन-जन से विस्मृत नहीं हो सकते, वे कभी नहीं मर सकते। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि लोकमान्य तिलक मर कर भी हमें जीवन का रहस्य सिखा गए। अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट के विरोध में बिना पंजीकरण कराएं मुंबई से "सत्याग्रही" नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भारतीय प्रेस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्रारंभ कर दिया। इसमें पाठकों के लिए यह सलाह छपी रहती थी- "कृपया इस समाचार पत्र को पढ़ें, प्रतिलिपि करें और मित्रों में प्रसारित करें और उनसे आग्रह करें कि इसकी प्रतिलिपि करें और प्रसारित करें।" [10]
1921 में उन्होंने अपने अंग्रेजी "यंग इंडिया" और गुजराती "नवजीवन" के साथ हिंदी में "नवजीवन" निकालना शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को "नवजीवन' हिंदी का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1932 तक गांधीजी ने इसका संपादन किया। उन्होंने इस पत्र को अपने सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का वाहक बनाया। उन्होंने "नवजीवन" के द्वारा गांव-गांव में स्वतंत्रता एवं जन-जागरण की अलख जगाई। 1932 में जब वे लंदन के गोलमेज अधिवेशन से लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और "नवजीवन" को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें एक रोचक सूचना यह भी छपी रहती थी कि यह समाचार पत्र नियमानुसार पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए इसका कोई वार्षिक शुल्क नहीं हो सकता है और न ही यह गारंटी दी जा सकती है कि यह पत्र बिना किसी व्यवधान के प्रकाशित होता रहेगा। इसके संपादक को सरकार के द्वारा किसी भी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है और सतत प्रकाशित होते रहने को सुनिश्चित करना तब तक असंभव है जब तक भारत इस अच्छी स्थिति में न हो जाए कि वह गिरफ्तार किए गए संपादकों के स्थान पर पर्याप्त संख्या में संपादकों को उपलब्ध कराने की स्थिति में हो, हम निरंतर एक के बाद एक संपादकों को प्राप्त करने के लिए कोई कसर न छोड़ेंगे। [11]
साप्ताहिक पत्र "हरिजन" का प्रकाशन पुणे से शनिवार दिनांक 11 फरवरी 1933 को हुआ। इस समाचार पत्र का प्रकाशन "हरिजन सेवक संघ" के तत्वावधान में हुआ जिसके अध्यक्ष सेठ घनश्याम दास बिरला थे। 4 फरवरी 1932 को "यंग इंडिया" और "नवजीवन" बंद हो गए तब महात्मा गांधी ने 8 जनवरी 1933 को यरवदा केंद्रीय जेल से घनश्याम दास बिरला को पत्र लिखा और हरिजना के प्रकाशन के बारे में विचार साझा किया। [12] "हरिजन" के प्रवेशांक में गांधीजी ने बताया कि चार वर्णों में जो समान अधिकार है उनका अधिकार हरिजनों को मिलना चाहिए। यह है- मंदिर प्रवेश, शालाओं में शिक्षा, सार्वजनिक कुओं, घाटों, तालाबों और नदियों में निस्तार सुविधा। गांधी के अनुसार हरिजन का शाब्दिक अर्थ है- “हरि का जन" सभी धर्मों में यही तथ्य वर्णित है कि हरि ही सबके मित्र पोषक रक्षक, स्वामी तथा सखा हैं। पहले "नवजीवन" में "अस्पृश्य' शब्द का प्रयोग हुआ था। [13]
गांधी ने "अस्पृश्य" के बदले गुजरात के संत कवि द्वारा प्रयुक्त “हरिजन" शब्द सार्थक को माना। दिल्ली से हिंदी में "हरिजन" का प्रकाशन "हरिजन सेवक" के नाम से श्री वियोगी हरि के संपादन में प्रारंभ किया गया। गुजराती में हरिजन का प्रकाशन हरिजन बंधु नाम से किया गया। 18 अगस्त 1942 को मुंबई कांग्रेस में जब महात्मा गांधी ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" का नारा देने के कारण गांधी गिरफ्तार कर लिए गए और "हरिजन" व "नवजीवन" प्रेस को जब्त कर लिया गया और समाचार पत्रों की पुरानी फाइलें नष्ट कर दी गयी। महात्मा गांधी जब जेल में ही थे तभी उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा जी का निधन हो गया। गांधीजी को 6 मई, 1944 को जेल से रिहा किया गया। [14] महात्मा गांधी ने समाचार पत्रों को पुनर्जीवित करने की इच्छा नहीं छोड़ी थी। फलतः 10 फरवरी 1946 को साढ़े तीन साल बाद "हरिजन" का प्रकाशन पुनः शुरू हुआ। गांधी ने 24 सितंबर 1938 को लिखा हरिजन अखबार नहीं है, यह एक व्यक्ति के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला विचार-पत्र है।" [15] महात्मा गांधी ने अनेक स्थानों पर स्वीकार किया कि “यंग इंडिया", "नवजीवन" "इंडियन ओपिनियन", "हरिजन" महज समाचार पत्र नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का निचोड़ (सार) था। महात्मा गांधी जी की पत्रिकाओं में नवजीवन, हरिजन, आज, सौराष्ट्र, भारतीय खादी समाचार, खादी जगत, खादी पत्राकार, नई तालीम, सबकी बोली, राष्ट्रभाषा, हिंदी प्रचारक, नया-हिंद, हरिजन सेवक, नशाबंदी संदेश, जीवन-साहित्य, गांधी-मार्ग, भारतीय-राय, सर्वोदय आदि प्रमुख हैं। वरिष्ठ पत्रकार एम. चेलापतिराव ने गांधी जी को महान पत्रकार माना है। उनके शब्दों में, "गांधी जी शायद सबसे महान पत्रकार हुए हैं और उन्होंने जिन साप्ताहिकों को चलाया और संपादित किया वे संभवतः विश्व के सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र है।" [16]
निष्कर्ष : गांधी जी का पत्रकार एवं संपादक के रूप में आज तक वास्तविक एवं शोधपरक मूल्यांकन नहीं हुआ है। उनके राजनीतिक मूल्यों और विचारधारा पर ही बहुत अधिक कार्य हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गांधी जी के पत्रकार एवं संपादक को नए आयाम में देखे और परिभाषित करें। उन्होंने पत्रकारिता के जो आदर्श बताए हैं और अपने जीवन काल में स्थापित किए है, उनका अनुसरण करें। 27 सितंबर 1925 को महात्मा गांधी ने "यंग इंडिया" में साफ शब्दों में लिखा है, "मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश स्वयं पत्रकारिता की खातिर नहीं किया है, बल्कि यह मेरे जीवन के ध्येय की पूर्ति में सहायक है, ऐसा मान कर किया है।“ यह पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि महात्मा गांधी के लिए पत्रकारिता उनके जीवन का ध्येय हासिल करने का सत्याग्रही मार्ग और सबसे बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक सहज साधन था। गांधी जी ने पत्र-पत्रिकाओं के सामने कुछ आदर्श रखे। वे चाहते थे कि विश्व की सभी पत्र-पत्रिकायें इन आदर्शों को निभाते हुए निकले। यह तय है कि लोगों को जागरूक करने के लिए गांधी जी ने पत्रकारिता का सहारा लिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करते हुए एक युग नायक की भूमिका निभाई। एक पत्रकार के रूप में गांधी युगों-युगों तक अपनी कृतियों में अमर रहेंगे।
सन्दर्भ :
- राम नारायण चौधरी,'बापू में क्या देखा, क्या समझा', नवजीवन प्रकाशन मंदिर , अहमदाबाद, 1954
- एम.के. गांधी, ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 1957
- रमेश जैन, ‘हिंदी पत्रकारिता: इतिहास और संरचना’, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2006
- रोमा रोलां, ‘महात्मा गांधी : जीवन और दर्शन’ - 2008
- साप्ताहिक पत्र, इंडियन ओपीनियन - 1905
- कमल किशोर गोयनका, ‘गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान’, नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
- आंचलिक पत्रकार; पत्रकारिता पर केन्द्रीत शोध पत्रिका, अंक सितंबर 1965
- हरिजन सेवक - 26 सतिंबर 1936, 7 अप्रैल 1946
- दैनिक समाचार पत्र - आज - 18 अगस्त 1967
- अंग्रेजी साप्ताहिक - यंग इंडिया - 3 अप्रैल 1924
- वी.जी देसाई, ‘गांधी एम.के. सत्याग्रह इन साऊथ अफ्रीका’, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद 1972
- रुडॉल्फंस् एल. आइ. एवं एस. एच., ‘पोस्टमॉर्डन गांधी : गांधी इन द वर्ल्ड एण्ड एट होम’, ओ.यू.पी., नई दिल्ली, 2005
- कृष्णा कृपलानी, ‘गांधी ऐ लाइफ’, एन. बी. टी., नई दिल्ली, 2008
- एस. एन. भट्टाचार्य, ‘महात्मा गांधी द जर्नलिस्ट’, ग्रीनवुड प्रेस, कनेक्टीकेट अमेरिका, 1984
- सुनील शर्मा, ‘जर्नलिस्ट गाँधी : सेलेक्टेड राइटिन्गस ऑफ गांधी’, यश प्रिन्टर्स, मुम्बई 1994
- श्यौराज सिंह, ‘अम्बेडकर गांधी और दलित पत्रकारिता’, अनामिका पब्लिशर्स, दिल्ली, 2008
बाला लखेंद्र
सह आचार्य, पत्रकारिता एवं जन-सम्प्रेषण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी – 221005
drbalalakhendra@gmail.com, 7985735729
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) से प्रकाशित पत्रिका
अपनी माटी (ISSN 2322-0724 Apni Maati) अंक-57, अक्टूबर-दिसम्बर, 2024 UGC CARE Approved Journal
इस अंक का सम्पादन : माणिक एवं विष्णु कुमार शर्मा छायांकन : कुंतल भारद्वाज(जयपुर)

एक टिप्पणी भेजें